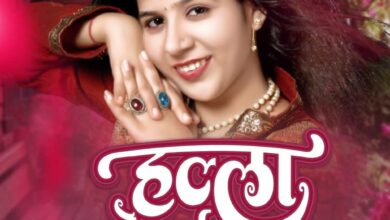झारखंड में बागवानी से 400 परिवारों की आजीविका को मिला नया आयाम
सरायकेला-खरसावां ज़िले में 400 से अधिक परिवार अब सुरक्षित और सस्टेनेबल आजीविका के लिए बागवानी आधारित खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह सकारात्मक बदलाव टाटा स्टील फाउंडेशन और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की साझेदारी से चल रही वाड़ी परियोजना के माध्यम से संभव हो पाया है

झारखंड में बागवानी से 400 परिवारों की आजीविका को मिला नया आयाम

्सरायकेला खरसावां- सरायकेला-खरसावां ज़िले में 400 से अधिक परिवार अब सुरक्षित और सस्टेनेबल आजीविका के लिए बागवानी आधारित खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह सकारात्मक बदलाव टाटा स्टील फाउंडेशन और नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की साझेदारी से चल रही वाड़ी परियोजना के माध्यम से संभव हो पाया है
2016-17 में शुरू की गई वाड़ी परियोजना का उद्देश्य छोटे बागानों का विकास करना है जिसमें मिट्टी और पानी का संरक्षण, अंतरवर्तीय फसलें नवीकरणीय ऊर्जा और बाज़ार तक बेहतर पहुंच भी शामिल है। केवल सरायकेला-खरसावां में ही 379 एकड़ ज़मीन को बागानों में बदला गया है। ज़्यादातर परिवार 1 से 2 एकड़ में आम और अमरूद को 70:30 के अनुपात में उगा रहे हैं। इससे हर परिवार की वार्षिक आय करीब 1.5 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जिससे उन समुदायों में नया आत्मविश्वास आया है जहां कभी खेती को भरोसेमंद नहीं माना जाता था
टाटा स्टील फाउंडेशन में एग्रीकल्चर हेड, अनंत सिंह कहते हैं, “कभी यहां खेती को अस्थिर और अनिश्चित माना जाता था क्योंकि यह खनन प्रधान इलाका है। लेकिन अब वही समुदाय खुद बदलाव की कहानी लिख रहा है बागवानी की योजना बना रहा है ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है और अंतरवर्तीय फसलों से अच्छी आमदनी भी कर रहा है।
फल और सब्जियों की कटाई के बाद उन्हें सही ढंग से संभालने के लिए किसानों को कोल्ड स्टोरेज और संग्रहण इकाइयों की सुविधा दी गई है। खेती से जुड़े उत्पाद सीधे स्थानीय बाजारों में बेचे जाते हैं, जैसे कि सिनी, सरायकेला, खरसावां, कांड्रा और गम्हरिया। फसल के पीक सीजन में किसान जमशेदपुर मंडी और रांची में नाबार्ड के मैंगो फेस्टिवल जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक भी अपनी उपज पहुंचाते हैं।
समुदाय स्तर पर बागवानी की देख रेख और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए 19 उद्यान विकास समितियाँ गठित की गई हैं। ये समितियाँ मिलकर 1.5 लाख रुपये का एक फंड संचालित करती हैं जिससे स्थानीय जरूरतों को पूरा किया जाता है यह मॉडल की भागीदारी-आधारित प्रकृति को दर्शाता है। अब तक 1,600 से अधिक किसानों को बागवानी, अंतरवर्तीय फसल और कीट प्रबंधन जैसी तकनीकी जानकारी दी जा चुकी है जिसमें आई सी ए आर रिसर्च कॉम्प्लेक्स, प्लांडू रांची और रामकृष्ण मिशन, रांची की अहम भूमिका रही है।
महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। इस पहल से जुड़ी 90% से अधिक महिलाओं ने बताया है कि अब उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्रता महसूस होती है। स्वयं सहायता समूहों और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से महिलाएं अब नर्सरी प्रबंधन, कंपोस्ट बनाने और अन्य छोटे निवेशों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर पा रही हैं।
व्यक्तिगत कहानियाँ इस बदलाव की असली तस्वीर पेश करती हैं। पहले शहर में दिहाड़ी मजदूरी करने वाली सुकुरमणी सोरेन ने जब अपने गाँव लौटकर 110 फलदार पेड़ लगाए, तो ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। अब वे आमदनी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि अपनी ज़मीन से आत्मनिर्भर हैं अंतरवर्तीय फसल और फल-सब्ज़ियों की बिक्री से उनकी सालाना आमदनी 10,000 रुपये से बढ़कर 48,000 हजार रुपये हो गई है। वह कहती हैं मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों को वह तकलीफ़ें न झेलनी पड़ें जो मैंने देखी हैं। अब वे स्कूल जाते हैं, अच्छा खाते हैं—क्योंकि मैंने गांव में रहकर अपने खेत से कमाया।” उनके इस कदम से न सिर्फ परिवार को राहत मिली, बल्कि गाँव में भूजल स्तर बढ़ा और लोगों को स्वच्छ पानी भी मिलने लगा।
मालती सोरेन, चार बेटियों की मां, कभी जंगल से लकड़ी चुनकर गुज़ारा करती थीं लेकिन आज सामुदायिक सहयोग से उन्होंने बकरी पालन शुरू किया है और अब उनके पास 1,600 से ज़्यादा बकरियाँ हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 1.44 लाख रुपये है। वे मुस्कुराकर कहती हैं “एक बकरी 10,000 रुपये में बिकती है और एक बकरी का बच्चा 8,000 रुपये में। इस आमदनी से मैंने अपनी बेटियों को पढ़ाया और अब गाँव की कई महिलाएं भी मुझे देख कर आगे बढ़ रही हैं।
किसानों को खेती से जुड़ी नई तकनीकों की ट्रेनिंग कोलाबेरा स्थित एग्रीकल्चर रिसोर्स सेंटर में दी जाती है, जहां पॉलीहाउस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां उन्हें बागवानी की योजना, मौसमी फसल की जानकारी और जलवायु के अनुसार स्मार्ट खेती के गुर सिखाए जाते हैं। पहले ही साल में कई परिवारों की आमदनी 50,000 रुपये तक पहुंच चुकी है जबकि पूरे ज़िले में बागवानी से कुल आमदनी 70 रुपये से 80 लाख रुपये तक हो गई है युवा किसान अर्जुन मार्डी और लखन किस्कु जैसे लोग यह साबित कर रहे हैं कि विविध खेती अपनाकर भी एक सफल और सस्टेनेबल जीवनशैली बनाई जा सकती है
उआल-बाहा एफपीसी के बोर्ड सदस्य अर्जुन ने अपने बागान को दो एकड़ तक बढ़ाया, इंटरक्रॉपिंग अपनाई और अपनी सालाना आमदनी 38,000 रुपये से बढ़ाकर 1.1 लाख रुपये कर ली। अब वे अपनी खेती की जानकारी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, “इस साल हमारा लक्ष्य ₹10 लाख का टर्नओवर है, जिसमें ₹3 लाख सिर्फ एनुअल फ्लावर शो से आएगा।” दूसरी ओर, लखन किस्कु ने बेहतर बीज, ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप जैसी सरकारी योजनाओं (जैसे पीएमकेएसवाई और पीएम-कुसुम) का लाभ उठाकर अपनी आय ₹29,000 से बढ़ाकर ₹65,000 कर ली है।
वाडी पहल सिर्फ आमदनी बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इससे विभिन्न मौसम में होनेवाले पलायन कम हुए हैं, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुंच मिल रही है, और गांवों में ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बाज़ार से जुड़ाव के ज़रिए समुदाय और भी मजबूत हो रहे हैं। अब कई परिवारों के लिए खेती एक भरोसेमंद और सस्टेनेबल भविष्य बन चुकी है